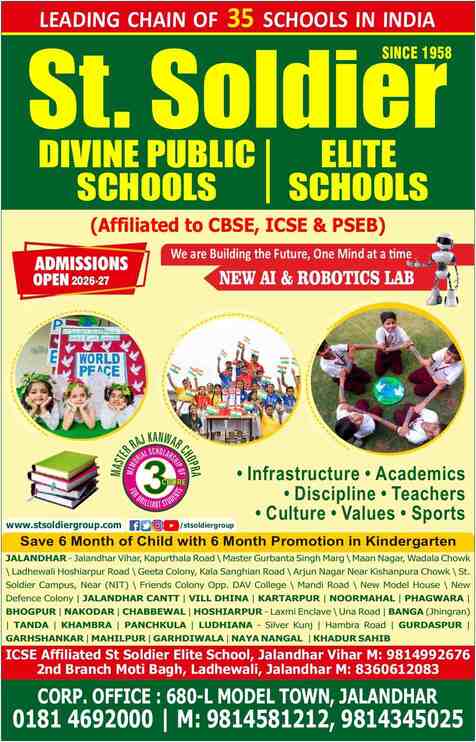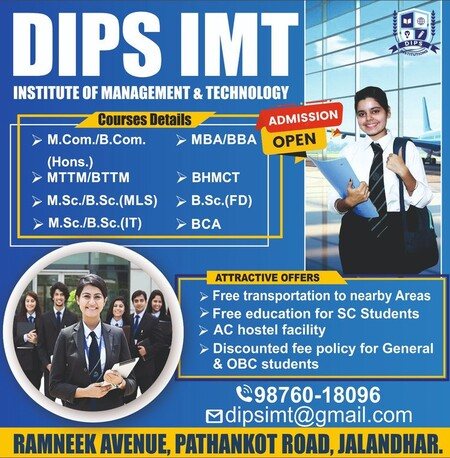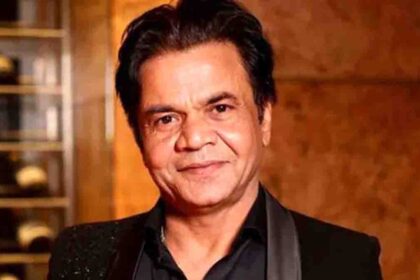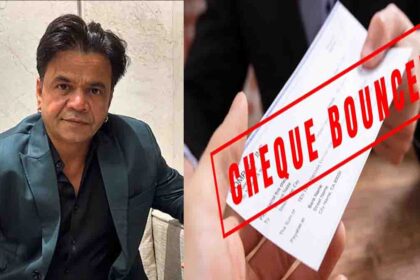डेली संवाद, मुंबई। Biopic Films: बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर्रहमान पर बांग्लादेश फिल्म डेवलेपमेंट कारपोरेशन 83 करोड़ रुपये में फिल्म बनाती है, ‘मुजीब-द मेकिंग आफ ए नेशन’, जिसमें आधा बजट यानी लगभग 40 करोड़ रुपये भारत सरकार देती है। अपनी खास शैली के लिए प्रतिष्ठित श्याम बेनेगल फिल्म का निर्देशन करते हैं।
यह भी पढ़ें : डेली संवाद की खबर का असर- माडल टाउन में अवैध बना Deck5 रेस्टोरेंट सील
हॉलीवुड की तो बात ही छोड़ दें, इसी के बरक्स देखें तो देश के सबसे सम्मानित राजनेता भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी पर केंद्रित फिल्म ‘मैं अटल हूं’ 10 करोड़ रुपये में और देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बायोपिक ‘पीएम नरेन्द्र मोदी’ लगभग आठ करोड़ रुपये में बनती है। …और हम कहते हैं कि भारत के राजनेताओं पर अच्छी बायोपिक क्यों नहीं बनती है।
भारतीय नेताओं पर बनी बायोपिक को दर्शक क्यों अस्वीकार कर देते हैं। रिचर्ड एटनबरो की ‘गांधी’ अभी भी स्मृतियों में है, आज से 42 साल पहले आई वह फिल्म 2.2 करोड़ डालर के बजट में बनी थी। आज भी यह फिल्म टेलीविजन पर आने लगती है तो दर्शक ठहर जाते हैं।
30 साल पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल पर बायोपिक ‘सरदार’ लगभग दो करोड़ रुपये के बजट में बनती है और 2000 में डा. बाबा साहेब आंबेडकर पर जब्बार पटेल नौ करोड़ रुपये में फिल्म बनाते हैं। यह सही है कि सिर्फ बजट से ही अच्छी फिल्म नहीं बनती, लेकिन यह भी सच है कि अच्छी फिल्म बनाने के लिए बजट की भी आवश्यकता होती है।
कमजोर हैं ये दो पहलू
किसी व्यक्ति पर जब कोई बायोपिक बनाना तय होता है तो सबसे पहली चीज होती है- रिसर्च और फिर पटकथा। कमाल यह कि सबसे कम खर्च इसी दोनों पक्ष पर होता है। बस अखबारी कतरनों के सहारे कोई कालजयी फिल्म की कल्पना भी कैसे की जा सकती है। आप फिल्म उतना भर ही दिखाकर नहीं बना सकते, जो पब्लिक डोमेन पर वर्षों से है। खासकर आज सूचनाओं के इस दौर में जब लोगों के पास जानकारियों का अंबार है, आखिर कुछ तो ऐसा हो जो दर्शकों को सिनेमाघर तक आने के लिए उत्साहित कर सके।
पौराणिक और ऐतिहासिक कथानक को हम बार-बार देख सकते हैं, लेकिन समकालीन खबरों से हम इतने विज्ञ होते हैं कि उसके प्रति रुचि बनाने के लिए कुछ खास करना जरूरी होता है, जहां हिंदी फिल्में कमजोर पड़ जाती हैं। बायोपिक में भी उसका जोर कथा से अधिक सूचनाओं पर होता है। किसी के जीवन को कथा में ढालने के लिए श्रम और समय की आवश्यकता होती है, हिंदी सिनेमा जिसकी जरूरत ही नहीं समझ पाता।
क्या करे अभिनेता
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के सर्वमान्य नेताओं में रहे। वे सत्ता में रहे, नहीं रहे, उनकी लोकप्रियता अप्रभावित रही। एक सर्वे के अनुसार, देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी पहले नंबर पर हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने तीसरे नंबर पर अपनी जगह सुरक्षित रखी है। एक राजनेता के साथ उनकी पहचान एक संवेदनशील कवि की भी रही है।
जमीन से उठकर दुनियाभर में अपने विचारों के साथ अपनी पहचान बनाने वाले इस विराट व्यक्तित्व को बायोपिक के नाम पर निबटाने की कोशिश की जाती है तो भला दर्शक क्यों स्वीकार करें। माना कि पंकज त्रिपाठी जैसे सिद्धहस्त अभिनेता उनके व्यक्तित्व को साकार करने में जी-जान लगा देते हैं, लेकिन कहने के लिए बात ही न हो तो अभिनेता क्या कर सकता है। ऐसा ही कुछ ‘पीएम नरेन्द्र मोदी’ के साथ दिखा।
क्या आश्चर्य नहीं कि नरेन्द्र मोदी जैसे जादुई व्यक्तित्व को साकार करने की जवाबदेही हिंदी सिनेमा में हाशिए पर पड़े अभिनेता विवेक ओबेराय को दी जाती है। यहां तक कि पटकथा और संवाद लिखने में भी विवेक हाथ आजमाते हैं। जिस व्यक्ति को देखने और सुनने दुनिया के किसी भी कोने में लाखों की संख्या में लोग टूट पड़ते हैं, उस पर इतने अनमने तरीके से कोई कैसे फिल्म परिकल्पित कर सकता है।

फिल्म 2019 के चुनाव के पहले प्रदर्शित करने की कोशिश की जाती है, लेकिन होती चुनाव के बाद है। नरेन्द्र मोदी तो अपार बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन ‘पीएम नरेन्द्र मोदी’ पूरी तरह खारिज कर दी जाती है। वाकई जब वास्तविक नरेन्द्र मोदी का जादुई आकर्षण सामने है, तो कोई एक कमजोर सी नकल क्यों देखे।
चेहरा नहीं कहानी की तलाश
वास्तव में बायोपिक के साथ फिल्मकार को अक्सर यह भ्रम होता है कि फिल्म तो उनके नाम पर चलेगी, जिन पर फिल्म बनी है। इसीलिए फिल्मकार का सारा जोर लुक की नकल उतारने पर रहता है। फिल्मकार यह समझ नहीं पाते कि दर्शक चेहरा देखने नहीं, कहानी देखने आ रहा है। दर्शक को सिनेमा में सिनेमा दिखाने की जवाबदेही तो सर्वप्रथम है, राजनेताओं पर बनी बायोपिक में अक्सर यह चूक होती है।
बाल ठाकरे पर केंद्रित दो फिल्म बनती है, एक रामगोपाल वर्मा बनाते हैं ‘सरकार’, दूसरी उनकी बायोपिक के रूप में बनती है ‘ठाकरे’। ‘सरकार’ पसंद की जाती है और ‘ठाकरे’ नकार दी जाती है। शायद इसलिए कि ‘सरकार’ एक औपन्यासिक कृति की तरह तैयार होती है, जबकि ‘ठाकरे’ शुष्क जीवनी की तरह। अमिताभ बच्चन ठाकरे नहीं लगते हुए भी ठाकरे की भूमिका में स्वीकार्य होते हैं, नवाजुद्दीन ठाकरे लगते हुए भी अस्वीकार्य।
कंगना काफी शिद्दत से जयललिता की बायोपिक ‘थलाइवी’ बनाती है, लेकिन जयललिता की अपार लोकप्रियता भी फिल्म को नहीं बचा पाती। आश्चर्य नहीं नितिन गडकरी की बायोपिक ‘गडकरी’ सिर्फ महाराष्ट्र के सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाती है।
यह भी पढ़ें: जालंधर के Board to Abroad के ट्रेवल एजैंट पर सनसनीखेज आरोप
भारत में समकालीन राजनेताओं पर बन रही बायोपिक की असफलता की सबसे बड़ी वजह ईमानदारी का अभाव दिखता है। कड़वा सच यही है कि हम नरेन्द्र मोदी या अटल बिहारी वाजपेयी पर इसलिए फिल्म नहीं बनाते कि उनके प्रति हमारी श्रद्धा या उनके विचारों के प्रति विश्वास है। बल्कि इसलिए बनाते हैं कि हमें उम्मीद होती है कि जैसे-तैसे भी फिल्म बन जाएगी तो व्यक्तिविशेष की लोकप्रियता फिल्म को संभाल लेगी!
जालंधर पुलिस ने कर डाला बड़ा कांड, लोग गुस्से में, देखें